“फूलों को कहाँ शौक़ बर्बादी का, भंवरों की फ़ितरत है चूसने वाली”
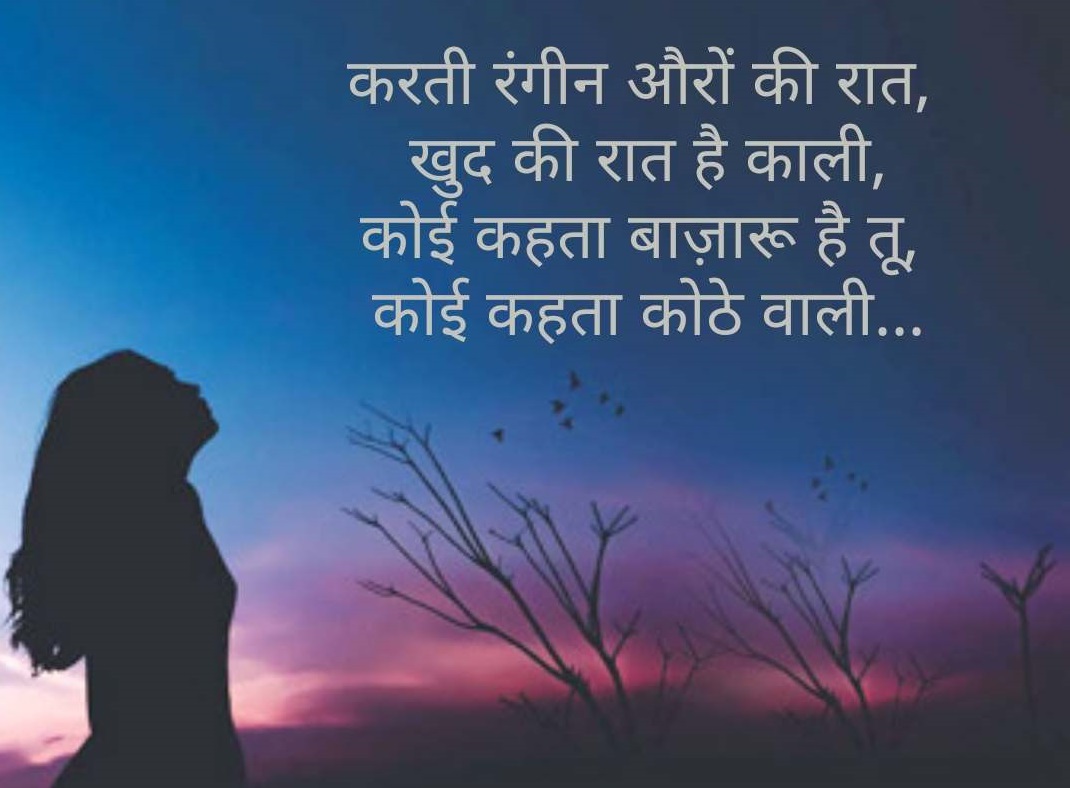 रुह उसकी छटपटाती पड़ी है खुद के वजूद को समेटे खामोशी ओढ़े एक गंदी नाली के कीड़े सी, आस-पास भूखे भेड़िए रेंगते है तन पिपासा की लालसा लिये। कहाँ शौक़ उसे कोठे वाली कहलाने का, पेट की आग के आगे परवश हो कर बिछ जाता है तन वहसिओं का बिछौना बनकर, उसके मन की पाक भूमि को कचोटती है ये क्रिया। किसको परवाह की दो बोल से नवाज़े शब्दों में पिरोकर हमदर्दी।
रुह उसकी छटपटाती पड़ी है खुद के वजूद को समेटे खामोशी ओढ़े एक गंदी नाली के कीड़े सी, आस-पास भूखे भेड़िए रेंगते है तन पिपासा की लालसा लिये। कहाँ शौक़ उसे कोठे वाली कहलाने का, पेट की आग के आगे परवश हो कर बिछ जाता है तन वहसिओं का बिछौना बनकर, उसके मन की पाक भूमि को कचोटती है ये क्रिया। किसको परवाह की दो बोल से नवाज़े शब्दों में पिरोकर हमदर्दी।
भाता है उसे खुद को पहने रहना क्यूँ कोई उसके अहसास को ओढ़े। दिन में नफ़रत भरी नज़रों के नज़रिये से तौलने वाले रात की रंगीनीयों में पैसों का ढ़ेर लगाते है। पी कर उसके हाथों से जाम ज़हर आँखों से घोलते है। कोई तो देह से परे उसकी पाक रुह को छूता जो पड़ी है अनछूई नीर सी निर्मल।
जो जीना चाहती है एक उजली ज़िस्त
दामन के पिछे धड़कते दिल की ख्वाहिशें जलती है तब, जब नोचते है बदन से मांस बिन अहसास के जैसे कोई तन को शीत करने वाला अग्नि शामक हो।
न….न मत देखो यूँ इस अखरती निगाहों से उसे ज़रा सी नर्म निगाह उसको भी भाती है, सिमटना देखो उसका, लजाती छुपाती पड़ी है। दे जो कोई उसकी परवाज़ को उड़ान का हौसला वह भी आसमान को बाँहों में समेटना चाहती है। क्या डाल सकता है कोई उसके बदन से गंदा कफ़न उखाड़कर दुपट्टा कोई पाक सा ?
“वो पथ नहीं भूली…..ज़िंदगी की भूलभूलैया ने गुम कर दिया है उसको” पेट की ज्वालाएँ उठती सीधा उसके उर को जलाती थी। दुन्यवी मायाजाल से बचती बचाती उलझती रही आख़िर बना दी गई कोठे की शान।
गंधडूबी काया के भीतर अश्कों से नहाती पाक साफ़ रूह पड़ी है। उपरी त्वचा के मोहाँध के हाथों रात की रंगीनियों के आगाज़ से लेकर सुबह तक ना जानें कितने हाथों से गुज़रती है उसकी काया चाय की किटली पर पड़े इकलौते अखब़ार कि तरह।
ये रंजो गम का सफ़र आसान नहीं रूह ही नहीं रूह की परछाई तक छलनी है उसकी। बस कोई उसके अहसास को हवा दो थोड़ी तो महसूस हो उसे की वह भी ज़िंदा है। ज़हर भी पीकर देखा ज़माने के हाथों। उसकी त्वचा पर असंख्य किड़े रेंगते अपनी छाप छोड़ गए है कोई ऐसी फूँक मारो की सारे दाग उड़ जाएं। आँचल उतारने वाले ही मिले, किसीने पाक दुपट्टे के दामन से उसके छरहरे बदन को ढ़कने की कोशिश तक नहीं कि। “कहाँ वह किसीकी अपनी थी”
 उसके रक्तकणों में बह रही तरह-तरह की हवस की बदबू खेल रही है। मणिकर्णिका से जब आख़री आँच उठेगी उसकी चिता से तब नासिका मत सिकुड़ लेना सब। काया भले ही मिट रही होगी कोठे वाली की पर उसकी छलनी रूह कान्हा की मुरली से प्रीत गुण्ठन करते अनंत के संग मिलन साध रही होगी।
उसके रक्तकणों में बह रही तरह-तरह की हवस की बदबू खेल रही है। मणिकर्णिका से जब आख़री आँच उठेगी उसकी चिता से तब नासिका मत सिकुड़ लेना सब। काया भले ही मिट रही होगी कोठे वाली की पर उसकी छलनी रूह कान्हा की मुरली से प्रीत गुण्ठन करते अनंत के संग मिलन साध रही होगी।
ना कोई महफ़िल का शोर होगा, ना उन्मादीत साँसों की गंध। झंझा से विमुख होते अन्तहीन निरवता के लय कणों में सोना है उसे मधु-प्रभात के इंतज़ार में हंमेशा के लिए। ज़िंदगी की आपाधापी को झेलते कोठे वाली का तन भले अपवित्र हो चुका आत्मा की शिखा पाक सी दिपदिपाती है। मजबूरी की मारी एक ज़िंदगी के तन को ही जाना सबने, मन की पवित्र जीवनी पढ़ने भीतर तक डूबकी कौन लगाता। कोठे वाली जो ठहरी बीवी थोड़ी थी किसीकी।
(भावना ठाकर, बेंगुलूरु)
Breaking News
- दामजीभाई एन्करवाला पर जारी किया गया डाक टिकट
- मुलायम सिंह यादव की शोभयात्रा का लेकर हुई चर्चा
- ई-रिक्शा, चार पहिया वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने की मांग
- खेलकूद प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाया जोश
- माताओं, बहनों ने कांग्रेसी नेता अतुल सिंह को बांधी राखी
- बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुआ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
- जीर्णोद्धार होने के बाद जनपद अपनी अलग पहचान बनाएगाः जयवीर सिंह
- आकर्षण झांकियों के साथ निकली भगवान श्रीकृष्ण की भव्य शोभायात्रा
- 25 रक्तदाताओं ने किया ब्लड डोनेट
- मुख्यमंत्री ने 646 करोड़ रुपये की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया
 Jansaamna
Jansaamna